मेरे सामने था , वो विशाल द्वार जिस के एक तरफ तीन बड़े बड़े अक्षर टिके थे - B I T. जैसे ही हमारी कार उस द्वार से अन्दर घुसी , याद आ गया वो बत्तीस साल पुराना क्षण , जब इन्जिनीरिंग का अंतिम पेपर देने की ख़ुशी मनाने के बाद बाहर निकले थे हम सभी मित्र ! जिंदगी इसी दरवाजे के बाहर तो हमारा इन्तजार कर रही थी .
 जैसे ही कार आगे बढ़ी , मैंने नजर डाली मेरी दाहिनी तरफ - और जैसी आशा थी वैसे ही नजर आया होस्टल -7 , और उसके बाद होस्टल -6 और उसके बाद होस्टल - 5. लेकिन उसके बाद जो नजर आया वो उन दिनों नहीं था . प्रताप , मेरे मित्र , सहपाठी और इस यात्रा के मेरे सूत्रधार , ने बताया की वो नए निर्माण है - एक गेस्ट हाउस और दो और नए होस्टल के रूप में .होस्टलों की संख्या 11 तक पहुँच चुकी है .
जैसे ही कार आगे बढ़ी , मैंने नजर डाली मेरी दाहिनी तरफ - और जैसी आशा थी वैसे ही नजर आया होस्टल -7 , और उसके बाद होस्टल -6 और उसके बाद होस्टल - 5. लेकिन उसके बाद जो नजर आया वो उन दिनों नहीं था . प्रताप , मेरे मित्र , सहपाठी और इस यात्रा के मेरे सूत्रधार , ने बताया की वो नए निर्माण है - एक गेस्ट हाउस और दो और नए होस्टल के रूप में .होस्टलों की संख्या 11 तक पहुँच चुकी है .

जो नहीं बदला वो था सड़क के दोनों तरफ हरे भरे लम्बे लम्बे पेड़ों से भरा जंगल , जिसके बीच की पगडंडियों से कभी पैदल कभी साईकिल पर जाते थे कोलेज की बिल्डिंग में क्लास के लिए . और जैसे ही वो रास्ता आगे बढ़ा , सामने नजर आई वो भव्य ईमारत जहाँ मैंने साढ़े चार सालों तक अलग अलग विषयों की कक्षाएं अटेंड की . आज भी उतनी ही प्रभावशाली जितनी उन दिनों होती थी . ईमारत के सामने हरे भरे दोनों घास के मैदान - जिन्हें हम कहते थे लोवर और अप्पर लॉन ! इन्ही मैदानों में न जाने कितनी बार क्रिकेट खेला , स्क्रीन लगाकर फ़िल्में देखी .
 दोनों तरफ दो दो विशाल होस्टल - 1 से लेकर 4 नंबर तक के . होस्टल चार के सामने से गुजरा तो अपना वो कमरा नजर आया जहाँ मैंने फोर्थ और फिफ्थ इयर की पढाई की . मेरे पास वाला कमरा हुआ करता , मेरे परम मित्र सुरेश बजाज का - जो इम्तिहान के दिन भी अपना आधे घंटा का पूजापाठ छोड़ने को तैयार नही होता था ; ये जानते हुए की उसे अभी भी कोलेज जाने के पहले मेरे साथ बैठ कर फ़ाइनल रिविजन करना है . मेरे कमरे के दूसरी तरफ था डार्क रूम , जिसमें हम घंटों अपनी खींची हुई तस्वीरों , ब्लैक एंड व्हाईट , को एनलार्ज और प्रिंट करते थे . मुझे याद है एक साल मैंने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में 5 अवार्ड जीते थे ; अभी भी सारे सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हैं . फोटोग्राफी याद करते ही मुझे याद आया , मेरा दोस्त प्रमोद अगरवाल , जो कुछ वर्षों पहले हम सब से बिछुड़ चूका है . प्रमोद का कमरा होस्टल की बिल्डिंग के दूसरी तरफ की एल विंग में था ; शायद सबसे सजा धजा कमरा वही हुआ करता था .
दोनों तरफ दो दो विशाल होस्टल - 1 से लेकर 4 नंबर तक के . होस्टल चार के सामने से गुजरा तो अपना वो कमरा नजर आया जहाँ मैंने फोर्थ और फिफ्थ इयर की पढाई की . मेरे पास वाला कमरा हुआ करता , मेरे परम मित्र सुरेश बजाज का - जो इम्तिहान के दिन भी अपना आधे घंटा का पूजापाठ छोड़ने को तैयार नही होता था ; ये जानते हुए की उसे अभी भी कोलेज जाने के पहले मेरे साथ बैठ कर फ़ाइनल रिविजन करना है . मेरे कमरे के दूसरी तरफ था डार्क रूम , जिसमें हम घंटों अपनी खींची हुई तस्वीरों , ब्लैक एंड व्हाईट , को एनलार्ज और प्रिंट करते थे . मुझे याद है एक साल मैंने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में 5 अवार्ड जीते थे ; अभी भी सारे सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हैं . फोटोग्राफी याद करते ही मुझे याद आया , मेरा दोस्त प्रमोद अगरवाल , जो कुछ वर्षों पहले हम सब से बिछुड़ चूका है . प्रमोद का कमरा होस्टल की बिल्डिंग के दूसरी तरफ की एल विंग में था ; शायद सबसे सजा धजा कमरा वही हुआ करता था .
 और फिर जब कोलेज की बिल्डिंग के आगे रुके , तो कितनी ही बातें जेहन में कौंध गयी . कोलेज के सामने बना वो सन डायल , रोज गार्डेन , सीढ़ियों के पास बना टेलीफोन एक्सचेज . टेलीफोन एक्सचेंज - सुनने में लगता है की कोई बहुत बड़ी चीज रही होगी ; लेकिन वो था 8 फुट बाई 6 फुट की एक कोठरी , जिसमें बैठा होता था एक टेलीफोन ओपरेटर , और उसके पास होते थे 2 टेलीफोन . पूरे कैम्पस में अगर किसी को भी फोन करना होता था तो वो आता था यहीं और अनुरोध करता था ओपरेटर से की उसका नंबर मिला कर देवे . एस टी डी नंबर का मतलब तो था वही सीढियों पर बैठ कर घंटों इन्तजार करना . आज के समय की सोचता हूँ तो लगता है की होस्टल के हर कमरे में कम से कम एक सेल फोन तो हर स्टुडेंट के पास होगा ही .
और फिर जब कोलेज की बिल्डिंग के आगे रुके , तो कितनी ही बातें जेहन में कौंध गयी . कोलेज के सामने बना वो सन डायल , रोज गार्डेन , सीढ़ियों के पास बना टेलीफोन एक्सचेज . टेलीफोन एक्सचेंज - सुनने में लगता है की कोई बहुत बड़ी चीज रही होगी ; लेकिन वो था 8 फुट बाई 6 फुट की एक कोठरी , जिसमें बैठा होता था एक टेलीफोन ओपरेटर , और उसके पास होते थे 2 टेलीफोन . पूरे कैम्पस में अगर किसी को भी फोन करना होता था तो वो आता था यहीं और अनुरोध करता था ओपरेटर से की उसका नंबर मिला कर देवे . एस टी डी नंबर का मतलब तो था वही सीढियों पर बैठ कर घंटों इन्तजार करना . आज के समय की सोचता हूँ तो लगता है की होस्टल के हर कमरे में कम से कम एक सेल फोन तो हर स्टुडेंट के पास होगा ही .
पहली मंजिल पर हुआ करता था वो बड़ा वाला कमरा जो अपने नंबर से ही जाना जाता था - 222 ; वो था पूरे कैम्पस का मनोरंजन केंद्र , क्योंकि महीने में एक दो फिल्म दिखाई जाती थी - नयी नहीं , उन दिनों से भी 10-20 साल पुरानी ! एक पुराने ज़माने का बड़ी बड़ी रीलों के चक्कों को घुमाने वाला प्रोजेक्टर - जिस पर फ़िल्में दिखाते थे हम लोग . और अगर कोई गाना या दृश्य अच्छा लगता तो जोरों की सीटियाँ बजती और फरमाइश होती - 'रिपीट ............" "रिपीट .................." और फिर जन आग्रह पर वो गीत या दृश्य दुबारा , तिबारा और कई बार तो चौबारा दिखाया जाता था . नयी फिल्मे देखने के लिए बस में बैठ कर रांची शहर जाना पड़ता था . वहां खड़े खड़े मन में आया , अब तो शायद हर कमरे में एक टी वी लगा होगा , जिस पर सभी देखते होंगे अपना मनचाहा चैनल . सचमुच सब कुछ बदल गया .
 फिर जब एक नम्बर होस्टल के पास पहुंचे तो मैंने प्रताप से कहा - यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं . गाडी से उतर कर हम घुसे . पहला बड़ा कमरा जहाँ उन दिनों होता था एक को ओपरेटिव स्टोर , जिसमें से खाने पीने के सामान की खुशबू आया करती थी . उसके बाद शुरू हुआ कमरों का सिलसिला - 8 नंबर - उपेन्द्र सिंह , 9 नंबर मोहमद जफ़र , 10 नंबर - मेरा जिगरी दोस्त अकिल अहमद- आजकल दुबई में है . और फिर 11 नंबर यानि मेरा कमरा , 12 नंबर - सुभाष महतो , 13 - बिभूति भूषण , अरे हाँ कुछ दिनों पहले ही फेसबुक पर मुलाकात हुई उससे - आर्मी में ब्रिगेडीअर बन गया . जैसे जैसे आगे बढ़ता गया याद आते गए सारे नाम - नवल द्विवेदी , भरद्वाज , सुशिल झुनझुनवाला , दिलीप मानकी , ........................शशांक प्रसाद ...............
फिर जब एक नम्बर होस्टल के पास पहुंचे तो मैंने प्रताप से कहा - यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं . गाडी से उतर कर हम घुसे . पहला बड़ा कमरा जहाँ उन दिनों होता था एक को ओपरेटिव स्टोर , जिसमें से खाने पीने के सामान की खुशबू आया करती थी . उसके बाद शुरू हुआ कमरों का सिलसिला - 8 नंबर - उपेन्द्र सिंह , 9 नंबर मोहमद जफ़र , 10 नंबर - मेरा जिगरी दोस्त अकिल अहमद- आजकल दुबई में है . और फिर 11 नंबर यानि मेरा कमरा , 12 नंबर - सुभाष महतो , 13 - बिभूति भूषण , अरे हाँ कुछ दिनों पहले ही फेसबुक पर मुलाकात हुई उससे - आर्मी में ब्रिगेडीअर बन गया . जैसे जैसे आगे बढ़ता गया याद आते गए सारे नाम - नवल द्विवेदी , भरद्वाज , सुशिल झुनझुनवाला , दिलीप मानकी , ........................शशांक प्रसाद ...............
और उसके बाद आ गया हमारा भोजन स्थल यानि की मेस ! यही वो जगह थी जहाँ घंटों दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलता था . उन दिनों हुआ करती थी स्टेनलेस की लम्बी टेबल जिसके दोनों तरफ जुड़े होते थे स्टेनलेस स्टील के ही गोल गोल स्टूल . किचन और हमारी टेबलों के बीच बना हुआ था एक पक्का काउंटर , जहाँ खड़ा रहता था मेस का मैनेजर ! शायद इस होस्टल में मैनेजर था प्रसाद . मेस की किचन से बन कर गरम गरम रोटियां बाहर आती - कई छोटे छोटे आदिवासी लड़के रोटियां परोसते . पूरे समय आवाजें आती रहती - ' ऐ बुतरू - रोटी ला ' , 'ऐ बुतरू - पानी ला ' . स्टेनलेस स्टील की वो बेंचें हटा दी गयी हैं. अब हैं होटलों जैसी टेबल और प्लास्टिक की मोल्डेड बकेट जो की कस दी गयी थी स्टील के स्टैंड के ऊपर . वहां तैनात एक सज्जन ने बताया की आज कल यहाँ सेल्फ सर्विस कर दी गयी है ; अब यहाँ बुतरू काम नहीं करते हैं . समझ में भी आ गया , बाल मजदूर की श्रेणी में आते हैं वो बुतरू .
जैसे ही मेस के बाहर निकला , तो याद आई - 'नानी' ! मेरी अपनी नानी नहीं , बल्कि हम सब की नानी . होस्टल के सभी बच्चे उस बुढिया को नानी बोलते थे . वो लंच के समय बाहर आकर , एक बोरी बिछाकर अपनी दुकान लगा लेती थी . उसकी बोरी पर बीचे होते थे - खीरे , टमाटर , आम , अंडे वैगरह ! स्वाद परिवर्तन के लिए हम लोग खरीद लेते थे सलाद की सामग्री . नानी का सम्बन्ध दिर्फ़ क्रय विक्रय तक सीमित नहीं था . वो सब से पूछती - ' आज तुम्हारा परचा कैसा हुआ ?' .....' अरे इतनी सर्दी लगी है , काढ़ा बनवा कर पी लो ' ........... आज पैसे नहीं है , कोई बात नहीं जब घर से आये तब दे देना ' - अपने घर वालों से दूर यहाँ भी था कोई घर वालों जैसा , जो चिंता करता था हम सबकी !
 अगले 15 मिनट में मैंने प्रताप के साथ चक्कर लगाया - अमीरचंद के कैंटीन का , नवनिर्मित होस्टल और ऑडिटोरियम की बिल्डिंगों का , एक नया फार्म का रिसर्च सेंटर दिखा . मुख्या बिल्डिंग के पीछे अब एक बैंक और ऐ टी एम् है , 3-4 दुकाने हैं . मेरा विभाग यानि प्रोडक्सन इन्गिनीरिंग का वर्कशॉप था वैसा का वैसा ! अन्दर घुसते ही कई लेथ मशीने , दाहिनी तरफ मेटलर्जी विभाग , पिछवाड़े में फौन्द्री .
अगले 15 मिनट में मैंने प्रताप के साथ चक्कर लगाया - अमीरचंद के कैंटीन का , नवनिर्मित होस्टल और ऑडिटोरियम की बिल्डिंगों का , एक नया फार्म का रिसर्च सेंटर दिखा . मुख्या बिल्डिंग के पीछे अब एक बैंक और ऐ टी एम् है , 3-4 दुकाने हैं . मेरा विभाग यानि प्रोडक्सन इन्गिनीरिंग का वर्कशॉप था वैसा का वैसा ! अन्दर घुसते ही कई लेथ मशीने , दाहिनी तरफ मेटलर्जी विभाग , पिछवाड़े में फौन्द्री .
कैंटीन के पास के चौराहे ने याद दिला दी वो प्राइवेट बस जिसमें या ये कहना चाहिए की जिस के ऊपर सवार होकर हम जाते थे रांची शहर .ऊपर का मतलब था बस की छत पर . आज सुबह एक विचित्र घटना हुई . रांची में मेरे अंकल की कार का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था . गाडी में थे मैं अंकल और मेरा कोलेज के दिनों का साथी रविन्द्र शर्मा . अंकल बार बार उस ड्राइवर को संबोधित कर रहे थे - सजाद के नाम से . मैंने रविन्द्र शर्मा से कहा - ' रविन्द्र , याद है हमारी बी आई टी वाली बस का ड्राइवर भी सजाद ही हुआ करता था . तभी अंकल के ड्राइवर ने कहा - ' जी वो मेरे पापा हैं ! वो बिनाका नाम की बस चलाते थे .' बस का नाम बताते ही शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही . 32 सालों बाद भी अगर कोई शक्श आपके मन में है तो जरूर कोई न कोई खास बात रही होगी उसमे . और इस प्रकार हमारी आत्मीयता हो गयी अंकल के ड्राइवर से .

सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं किसी टाइम मशीन पर सवार होकर 32 वर्षों पीछे चला गया था . मष्तिष्क में न जाने कितने दबे हुए नाम बाहर निकल आये . न जाने कितनी ही घटनाएँ कौंध गयी . एक न भूल पाने वाला दिन बीता आज . थैंक यु प्रताप !
 जैसे ही कार आगे बढ़ी , मैंने नजर डाली मेरी दाहिनी तरफ - और जैसी आशा थी वैसे ही नजर आया होस्टल -7 , और उसके बाद होस्टल -6 और उसके बाद होस्टल - 5. लेकिन उसके बाद जो नजर आया वो उन दिनों नहीं था . प्रताप , मेरे मित्र , सहपाठी और इस यात्रा के मेरे सूत्रधार , ने बताया की वो नए निर्माण है - एक गेस्ट हाउस और दो और नए होस्टल के रूप में .होस्टलों की संख्या 11 तक पहुँच चुकी है .
जैसे ही कार आगे बढ़ी , मैंने नजर डाली मेरी दाहिनी तरफ - और जैसी आशा थी वैसे ही नजर आया होस्टल -7 , और उसके बाद होस्टल -6 और उसके बाद होस्टल - 5. लेकिन उसके बाद जो नजर आया वो उन दिनों नहीं था . प्रताप , मेरे मित्र , सहपाठी और इस यात्रा के मेरे सूत्रधार , ने बताया की वो नए निर्माण है - एक गेस्ट हाउस और दो और नए होस्टल के रूप में .होस्टलों की संख्या 11 तक पहुँच चुकी है .
जो नहीं बदला वो था सड़क के दोनों तरफ हरे भरे लम्बे लम्बे पेड़ों से भरा जंगल , जिसके बीच की पगडंडियों से कभी पैदल कभी साईकिल पर जाते थे कोलेज की बिल्डिंग में क्लास के लिए . और जैसे ही वो रास्ता आगे बढ़ा , सामने नजर आई वो भव्य ईमारत जहाँ मैंने साढ़े चार सालों तक अलग अलग विषयों की कक्षाएं अटेंड की . आज भी उतनी ही प्रभावशाली जितनी उन दिनों होती थी . ईमारत के सामने हरे भरे दोनों घास के मैदान - जिन्हें हम कहते थे लोवर और अप्पर लॉन ! इन्ही मैदानों में न जाने कितनी बार क्रिकेट खेला , स्क्रीन लगाकर फ़िल्में देखी .
 दोनों तरफ दो दो विशाल होस्टल - 1 से लेकर 4 नंबर तक के . होस्टल चार के सामने से गुजरा तो अपना वो कमरा नजर आया जहाँ मैंने फोर्थ और फिफ्थ इयर की पढाई की . मेरे पास वाला कमरा हुआ करता , मेरे परम मित्र सुरेश बजाज का - जो इम्तिहान के दिन भी अपना आधे घंटा का पूजापाठ छोड़ने को तैयार नही होता था ; ये जानते हुए की उसे अभी भी कोलेज जाने के पहले मेरे साथ बैठ कर फ़ाइनल रिविजन करना है . मेरे कमरे के दूसरी तरफ था डार्क रूम , जिसमें हम घंटों अपनी खींची हुई तस्वीरों , ब्लैक एंड व्हाईट , को एनलार्ज और प्रिंट करते थे . मुझे याद है एक साल मैंने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में 5 अवार्ड जीते थे ; अभी भी सारे सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हैं . फोटोग्राफी याद करते ही मुझे याद आया , मेरा दोस्त प्रमोद अगरवाल , जो कुछ वर्षों पहले हम सब से बिछुड़ चूका है . प्रमोद का कमरा होस्टल की बिल्डिंग के दूसरी तरफ की एल विंग में था ; शायद सबसे सजा धजा कमरा वही हुआ करता था .
दोनों तरफ दो दो विशाल होस्टल - 1 से लेकर 4 नंबर तक के . होस्टल चार के सामने से गुजरा तो अपना वो कमरा नजर आया जहाँ मैंने फोर्थ और फिफ्थ इयर की पढाई की . मेरे पास वाला कमरा हुआ करता , मेरे परम मित्र सुरेश बजाज का - जो इम्तिहान के दिन भी अपना आधे घंटा का पूजापाठ छोड़ने को तैयार नही होता था ; ये जानते हुए की उसे अभी भी कोलेज जाने के पहले मेरे साथ बैठ कर फ़ाइनल रिविजन करना है . मेरे कमरे के दूसरी तरफ था डार्क रूम , जिसमें हम घंटों अपनी खींची हुई तस्वीरों , ब्लैक एंड व्हाईट , को एनलार्ज और प्रिंट करते थे . मुझे याद है एक साल मैंने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में 5 अवार्ड जीते थे ; अभी भी सारे सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हैं . फोटोग्राफी याद करते ही मुझे याद आया , मेरा दोस्त प्रमोद अगरवाल , जो कुछ वर्षों पहले हम सब से बिछुड़ चूका है . प्रमोद का कमरा होस्टल की बिल्डिंग के दूसरी तरफ की एल विंग में था ; शायद सबसे सजा धजा कमरा वही हुआ करता था . और फिर जब कोलेज की बिल्डिंग के आगे रुके , तो कितनी ही बातें जेहन में कौंध गयी . कोलेज के सामने बना वो सन डायल , रोज गार्डेन , सीढ़ियों के पास बना टेलीफोन एक्सचेज . टेलीफोन एक्सचेंज - सुनने में लगता है की कोई बहुत बड़ी चीज रही होगी ; लेकिन वो था 8 फुट बाई 6 फुट की एक कोठरी , जिसमें बैठा होता था एक टेलीफोन ओपरेटर , और उसके पास होते थे 2 टेलीफोन . पूरे कैम्पस में अगर किसी को भी फोन करना होता था तो वो आता था यहीं और अनुरोध करता था ओपरेटर से की उसका नंबर मिला कर देवे . एस टी डी नंबर का मतलब तो था वही सीढियों पर बैठ कर घंटों इन्तजार करना . आज के समय की सोचता हूँ तो लगता है की होस्टल के हर कमरे में कम से कम एक सेल फोन तो हर स्टुडेंट के पास होगा ही .
और फिर जब कोलेज की बिल्डिंग के आगे रुके , तो कितनी ही बातें जेहन में कौंध गयी . कोलेज के सामने बना वो सन डायल , रोज गार्डेन , सीढ़ियों के पास बना टेलीफोन एक्सचेज . टेलीफोन एक्सचेंज - सुनने में लगता है की कोई बहुत बड़ी चीज रही होगी ; लेकिन वो था 8 फुट बाई 6 फुट की एक कोठरी , जिसमें बैठा होता था एक टेलीफोन ओपरेटर , और उसके पास होते थे 2 टेलीफोन . पूरे कैम्पस में अगर किसी को भी फोन करना होता था तो वो आता था यहीं और अनुरोध करता था ओपरेटर से की उसका नंबर मिला कर देवे . एस टी डी नंबर का मतलब तो था वही सीढियों पर बैठ कर घंटों इन्तजार करना . आज के समय की सोचता हूँ तो लगता है की होस्टल के हर कमरे में कम से कम एक सेल फोन तो हर स्टुडेंट के पास होगा ही .पहली मंजिल पर हुआ करता था वो बड़ा वाला कमरा जो अपने नंबर से ही जाना जाता था - 222 ; वो था पूरे कैम्पस का मनोरंजन केंद्र , क्योंकि महीने में एक दो फिल्म दिखाई जाती थी - नयी नहीं , उन दिनों से भी 10-20 साल पुरानी ! एक पुराने ज़माने का बड़ी बड़ी रीलों के चक्कों को घुमाने वाला प्रोजेक्टर - जिस पर फ़िल्में दिखाते थे हम लोग . और अगर कोई गाना या दृश्य अच्छा लगता तो जोरों की सीटियाँ बजती और फरमाइश होती - 'रिपीट ............" "रिपीट .................." और फिर जन आग्रह पर वो गीत या दृश्य दुबारा , तिबारा और कई बार तो चौबारा दिखाया जाता था . नयी फिल्मे देखने के लिए बस में बैठ कर रांची शहर जाना पड़ता था . वहां खड़े खड़े मन में आया , अब तो शायद हर कमरे में एक टी वी लगा होगा , जिस पर सभी देखते होंगे अपना मनचाहा चैनल . सचमुच सब कुछ बदल गया .
 फिर जब एक नम्बर होस्टल के पास पहुंचे तो मैंने प्रताप से कहा - यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं . गाडी से उतर कर हम घुसे . पहला बड़ा कमरा जहाँ उन दिनों होता था एक को ओपरेटिव स्टोर , जिसमें से खाने पीने के सामान की खुशबू आया करती थी . उसके बाद शुरू हुआ कमरों का सिलसिला - 8 नंबर - उपेन्द्र सिंह , 9 नंबर मोहमद जफ़र , 10 नंबर - मेरा जिगरी दोस्त अकिल अहमद- आजकल दुबई में है . और फिर 11 नंबर यानि मेरा कमरा , 12 नंबर - सुभाष महतो , 13 - बिभूति भूषण , अरे हाँ कुछ दिनों पहले ही फेसबुक पर मुलाकात हुई उससे - आर्मी में ब्रिगेडीअर बन गया . जैसे जैसे आगे बढ़ता गया याद आते गए सारे नाम - नवल द्विवेदी , भरद्वाज , सुशिल झुनझुनवाला , दिलीप मानकी , ........................शशांक प्रसाद ...............
फिर जब एक नम्बर होस्टल के पास पहुंचे तो मैंने प्रताप से कहा - यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं . गाडी से उतर कर हम घुसे . पहला बड़ा कमरा जहाँ उन दिनों होता था एक को ओपरेटिव स्टोर , जिसमें से खाने पीने के सामान की खुशबू आया करती थी . उसके बाद शुरू हुआ कमरों का सिलसिला - 8 नंबर - उपेन्द्र सिंह , 9 नंबर मोहमद जफ़र , 10 नंबर - मेरा जिगरी दोस्त अकिल अहमद- आजकल दुबई में है . और फिर 11 नंबर यानि मेरा कमरा , 12 नंबर - सुभाष महतो , 13 - बिभूति भूषण , अरे हाँ कुछ दिनों पहले ही फेसबुक पर मुलाकात हुई उससे - आर्मी में ब्रिगेडीअर बन गया . जैसे जैसे आगे बढ़ता गया याद आते गए सारे नाम - नवल द्विवेदी , भरद्वाज , सुशिल झुनझुनवाला , दिलीप मानकी , ........................शशांक प्रसाद ...............और उसके बाद आ गया हमारा भोजन स्थल यानि की मेस ! यही वो जगह थी जहाँ घंटों दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलता था . उन दिनों हुआ करती थी स्टेनलेस की लम्बी टेबल जिसके दोनों तरफ जुड़े होते थे स्टेनलेस स्टील के ही गोल गोल स्टूल . किचन और हमारी टेबलों के बीच बना हुआ था एक पक्का काउंटर , जहाँ खड़ा रहता था मेस का मैनेजर ! शायद इस होस्टल में मैनेजर था प्रसाद . मेस की किचन से बन कर गरम गरम रोटियां बाहर आती - कई छोटे छोटे आदिवासी लड़के रोटियां परोसते . पूरे समय आवाजें आती रहती - ' ऐ बुतरू - रोटी ला ' , 'ऐ बुतरू - पानी ला ' . स्टेनलेस स्टील की वो बेंचें हटा दी गयी हैं. अब हैं होटलों जैसी टेबल और प्लास्टिक की मोल्डेड बकेट जो की कस दी गयी थी स्टील के स्टैंड के ऊपर . वहां तैनात एक सज्जन ने बताया की आज कल यहाँ सेल्फ सर्विस कर दी गयी है ; अब यहाँ बुतरू काम नहीं करते हैं . समझ में भी आ गया , बाल मजदूर की श्रेणी में आते हैं वो बुतरू .
जैसे ही मेस के बाहर निकला , तो याद आई - 'नानी' ! मेरी अपनी नानी नहीं , बल्कि हम सब की नानी . होस्टल के सभी बच्चे उस बुढिया को नानी बोलते थे . वो लंच के समय बाहर आकर , एक बोरी बिछाकर अपनी दुकान लगा लेती थी . उसकी बोरी पर बीचे होते थे - खीरे , टमाटर , आम , अंडे वैगरह ! स्वाद परिवर्तन के लिए हम लोग खरीद लेते थे सलाद की सामग्री . नानी का सम्बन्ध दिर्फ़ क्रय विक्रय तक सीमित नहीं था . वो सब से पूछती - ' आज तुम्हारा परचा कैसा हुआ ?' .....' अरे इतनी सर्दी लगी है , काढ़ा बनवा कर पी लो ' ........... आज पैसे नहीं है , कोई बात नहीं जब घर से आये तब दे देना ' - अपने घर वालों से दूर यहाँ भी था कोई घर वालों जैसा , जो चिंता करता था हम सबकी !
 अगले 15 मिनट में मैंने प्रताप के साथ चक्कर लगाया - अमीरचंद के कैंटीन का , नवनिर्मित होस्टल और ऑडिटोरियम की बिल्डिंगों का , एक नया फार्म का रिसर्च सेंटर दिखा . मुख्या बिल्डिंग के पीछे अब एक बैंक और ऐ टी एम् है , 3-4 दुकाने हैं . मेरा विभाग यानि प्रोडक्सन इन्गिनीरिंग का वर्कशॉप था वैसा का वैसा ! अन्दर घुसते ही कई लेथ मशीने , दाहिनी तरफ मेटलर्जी विभाग , पिछवाड़े में फौन्द्री .
अगले 15 मिनट में मैंने प्रताप के साथ चक्कर लगाया - अमीरचंद के कैंटीन का , नवनिर्मित होस्टल और ऑडिटोरियम की बिल्डिंगों का , एक नया फार्म का रिसर्च सेंटर दिखा . मुख्या बिल्डिंग के पीछे अब एक बैंक और ऐ टी एम् है , 3-4 दुकाने हैं . मेरा विभाग यानि प्रोडक्सन इन्गिनीरिंग का वर्कशॉप था वैसा का वैसा ! अन्दर घुसते ही कई लेथ मशीने , दाहिनी तरफ मेटलर्जी विभाग , पिछवाड़े में फौन्द्री .कैंटीन के पास के चौराहे ने याद दिला दी वो प्राइवेट बस जिसमें या ये कहना चाहिए की जिस के ऊपर सवार होकर हम जाते थे रांची शहर .ऊपर का मतलब था बस की छत पर . आज सुबह एक विचित्र घटना हुई . रांची में मेरे अंकल की कार का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था . गाडी में थे मैं अंकल और मेरा कोलेज के दिनों का साथी रविन्द्र शर्मा . अंकल बार बार उस ड्राइवर को संबोधित कर रहे थे - सजाद के नाम से . मैंने रविन्द्र शर्मा से कहा - ' रविन्द्र , याद है हमारी बी आई टी वाली बस का ड्राइवर भी सजाद ही हुआ करता था . तभी अंकल के ड्राइवर ने कहा - ' जी वो मेरे पापा हैं ! वो बिनाका नाम की बस चलाते थे .' बस का नाम बताते ही शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही . 32 सालों बाद भी अगर कोई शक्श आपके मन में है तो जरूर कोई न कोई खास बात रही होगी उसमे . और इस प्रकार हमारी आत्मीयता हो गयी अंकल के ड्राइवर से .

सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं किसी टाइम मशीन पर सवार होकर 32 वर्षों पीछे चला गया था . मष्तिष्क में न जाने कितने दबे हुए नाम बाहर निकल आये . न जाने कितनी ही घटनाएँ कौंध गयी . एक न भूल पाने वाला दिन बीता आज . थैंक यु प्रताप !
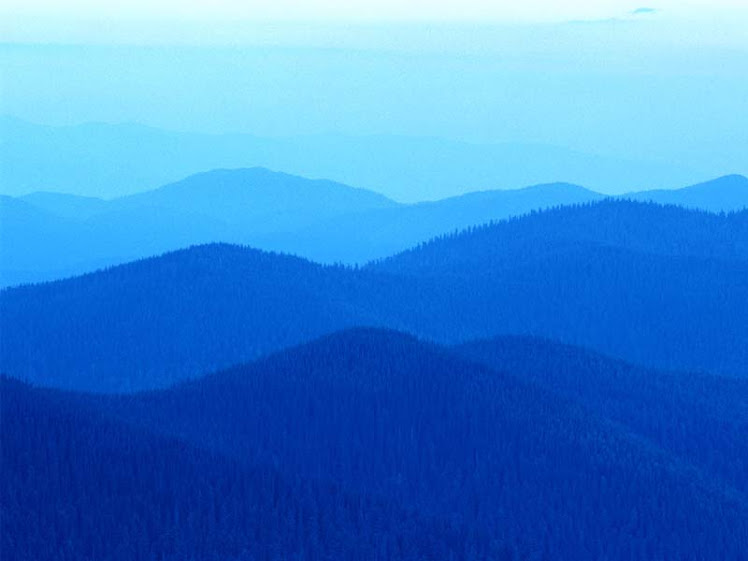

...nicely expressed blog!...had a wonderful feeling after taking Mahendra for a trip down the memory lane!!
ReplyDeletepratap